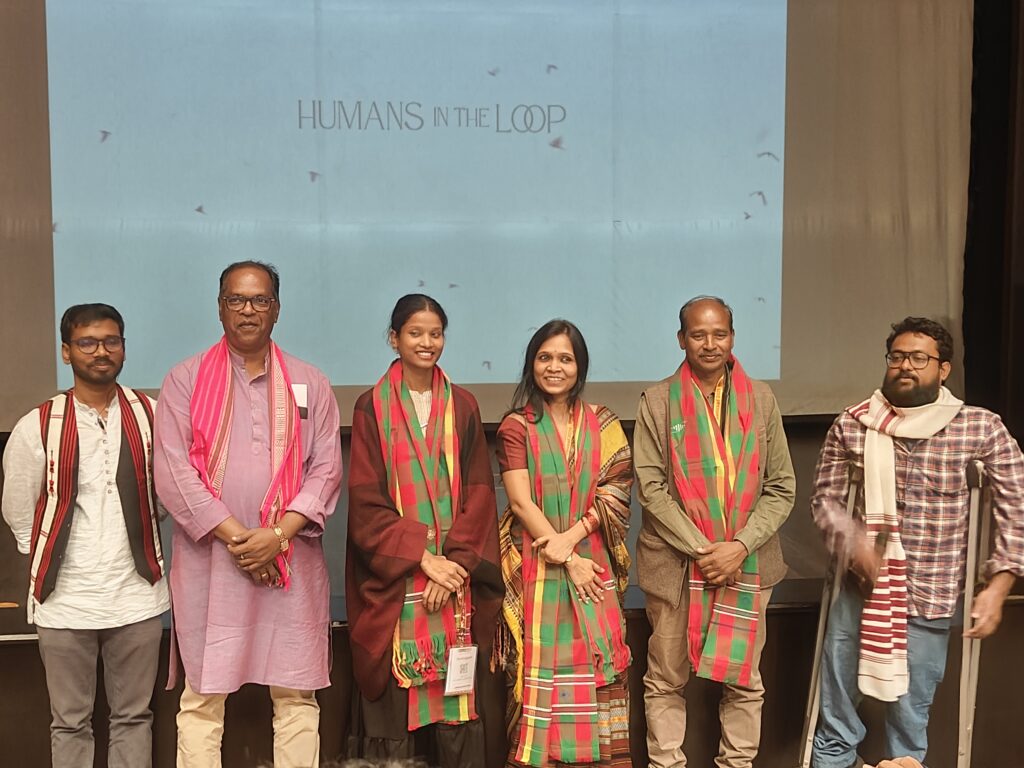ह्यूमंस इन द लूप
‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म के बारे में लिखने बैठी हूँ तो सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। इसे देखते हुए कहीं गहराई में महसूस होता रहा कि जीवन की अनुगूंज हमारे साथ हमेशा चलती रहती है कई बार हम उसे रेखांकित नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते पर वो गहरी जड़ों के मूलरंध्रों में रिसती हुई हमारी संवेदनाओं को पोषित कर रही होती है बिलकुल इसी एहसास से गुज़रना हुआ जब इस फिल्म को पहली बार देखा और उसके बाद जब और बार देखा तो।
संवेदनाओं और रिश्तों की
कुदरत से अपनेपन की
सामाजिक रिश्तों में जेंडर लेंस, समुदाय, परिवार , पुरखों की
बच्चों के मनोविज्ञान की
बाज़ार,कॉर्पोरेट के विस्तार की
कर्मचारियों की सीमाओं की
और
गाँव और जंगल की गहन बुनावट से गुंथी
ह्यूमंस इन द लूप एक ऐसी कहानी है जिसे हम इनसे इतर भी कई लेंस से देख सकते हैं ये हम दर्शको पर निर्भर करता है कि हम फिल्म को कैसे देखें , समझें और बरतें।
इस फिल्म के क़िस्सागो अरण्य सहाय ने सूक्ष्मता से जिस तरह से कहानी को गूंथा है वो मिसाल है जिसमें बतौर निर्देशक ने किस तरह से जटिल पाश को पहले फिल्म में गूंथा और फिर धीरे-धीरे एक-एक चरित्र की परत दर परत खोलते हुए कहानी को उस बिन्दु तक पहुंचाया जहां पहुंचकर हम एक गहरी अनुभूति के साथ भरे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं।
पाश में बंधे जीवन के जंगल में विचरते हम दुनियावी सभ्यता की वो हस्ती हैं जो अपने आप को सर्वोच्च मानने का गुमान करती हैं और दावा करती हैं कि हम इस धरती के सर्वेसर्वा हैं। इस गुमान को जीने वालों के लिए यह ज़रूरी फिल्म है जहां यह फिल्म धीमे से ,हौले से बाज़ार और तकनीक के बेढब किलों को पारकर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश होती है जो उनकी कहानी कहती है जो बाज़ारी संबंधों से इतर अपने लोकज्ञान और जीवन दर्शन से पोषित हैं जो गर्व, घमंड और श्रेष्ठता बोध से परे प्रकृति के साथ जीवन जी रहे हैं और प्रकृति के साथ साहचर्य का ऐसा अनूठा उदाहरण पेश करते हैं जिनकी संस्कृति से आप अछूते नहीं रह सकते।
‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म में आदिवासी जीवन दर्शन को आत्मसात करना दिल को छू गया। जीवन जीने का सलीका जो बचपन से एक हरे बीज सा रोप दिया जाता है वो किसी पुरखे के प्राचीन-विशाल पेड़ की तरह जंगल की हर पगडंडी, पेड़-पौधों ,नदी-पोखर, जीव-जंतुओं, पहाड़ और चट्टानों के साथ आकाश और पंछियों में उड़ता हुआ अपने जीवन की विशालता से परिचित कराता है।
फिल्म के पहले दृश्य और अंतिम दृश्य के बीच जैसे हम कभी खत्म न हो पाने वाले सेतु से गुज़रते हुए हरेपन से भरे एहसास से भर जाते हैं। एक कविता जो पहले दृश्य में चट्टान में कान लगाकर सुनती नेहमा के माध्यम से हम दर्शको तक पहुँचती है और हम इस कविता के राग में बंधे हुए थोड़ा और मनुष्यत्व की ओर बढ़ पाते हैं।
पूरी फिल्म की बुनावट ऐसी है जिसमें एक तरफ हर ओर बंधन महसूस होते हैं पर दूसरी तरफ एक खिड़की भी खुलती है जो खुले आकाश की तरफ खुलती है जिसमें पंछी जैसे उड़ने की चाहत विसरित होती है और पाश टूटकर आज़ादी का एहसास कराते हैं।
बचपन के खेल में पहला आदिवासी दर्शन कि धरती की हर चीज़ चाहे वो पत्थर हो, कटवा धान हो या सूखी लकड़ियां हों सबमें जान होती है ये दर्शन असल में हमें मनुष्यता की तरफ आगे ले जाने का रास्ता है कि हम संवेदनशील बनें। इसी क्रम में आगे यह कि पुरखों ने हर गुफ़ा में चित्र बनाए हैं जिसके पीछे यह बात छिपी है अपनी जानकारी को, ज्ञान को आगे ले जाने की चाह। तीसरा संवाद नेहमा का धानु के साथ कि शकरकंदी कैसे निकालना है और उसे कैसे फिर अपनी जगह में संजो देना है इसके बाद शैवाल,काई को जीवनदाता बताना कि जिनकी वजह से हम सब सांस ले पाते हैं। इस जगह में विशाल पेड़ की जगह चट्टानों में उभर आये इन सूक्ष्म काई का ज़िक्र ये दर्शाता है कि बड़े के साथ सूक्ष्म की उपस्थिति भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और इन सबसे बढ़कर लोकज्ञान में वैज्ञानिक चेतना की उपस्थिति। इल्ली को देख यह बताना कि ये पत्तियों के दोस्त हैं, ये सारे संवाद और दृश्य एक ऐसी दुनिया से शहरी संस्कृति को परिचित करता है जो आज भागती ज़िंदगी में ठहरकर सोचने-देखने और विचारने की क्षमता से परे हो चुका है। प्रकृति में रहने वाले हमारे पुरखे आदिवासियों को जो दुनिया के मूलनिवासी हैं हम शहरी लोग उनके जीवन को ठहराव से भरा और पिछड़ा मानते हैं जबकि प्रकृति को जीवन सत्य मानने वाले जंगल के इन दावेदारों की वजह से ही हम आज ज़िंदा है।
पूरी फिल्म के हर फ्रेम में नेहमा,धानु,मालती,रौशन और अन्य चरित्रों की उंगली पकड़कर प्रकृति साथ चली है। जैसे प्रकृति अपने किये को गाती नहीं यानी बखान (मुंह मियाँ मिट्ठू ) नहीं करती बिलकुल वैसे ही इस फिल्म की केंद्रीय पात्र नेहमा भी बस ज़रूरी संवाद के साथ अपने चरित्र को मौन में अभिनीत की हैं , प्रकृति के साथ सामंजस्य और रिश्ते को और नेहमा के शर्मीले व्यवहार के लिए साही से दोस्ती वो प्रतीक बना है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते जब तक कि जंगल में जीवन न गुज़ारें। दोस्ती के लिए मूक जानवर और प्रकृति के सम्बन्ध शहरी और पूंजीवादी सोच में डूबे लोग भूल चुके हैं इसलिए साही और नेहमा की दोस्ती का प्रतीक वो सीख है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौट सकें।
जब पहली बार फिल्म देखी तब मुझे सोनल मधुशंकर के बारे में जानकारी नहीं थी बस फिल्म दिलो – दिमाग में किसी सोते सी रिसती रही और उसके बाद जमशेदपुर में स्क्रीनिंग के समय उनके साथ फिल्म देखने का मौक़ा लगा और उसके बाद उन्हें सुनने का तो फिल्म के साथ उनके चरित्र के प्रति गम्भीरता से न्याय कर पाने की एक और वजह मिली हालांकि यहां यह भी कहाँ ज़रूरी है कि किसी किरदार को निभाने के लिए कलाकार की विशेष पहचान से ज़्यादा ज़रूरी उसकी संवेदनशीलता और अभिनय क्षमता का योगदान होता है। बहरहाल सोनल मधुशंकर उर्फ़ नेहमा ने स्क्रीनिंग के बाद कहा –
‘ कार्यशाला के दौरान फिल्म का आइडिया आया। करिश्मा मेहरोत्रा का ह्यूमन टच एक आलेख लिखा जिससे यह फिल्म प्रेरित है। ऑडिशन देकर इस फिल्म में एंट्री हुई। नेहमा का चरित्र जब सामने आया तो पता चला कि नेहमा आदिवासी है , मैं ट्राइबल नहीं पर दलित समुदाय यानी शेडयूल कास्ट से आती हूँ। जीवन की कठिनाइयों को समझती हूँ कि अगड़ी जातियों से अंतर/भेदभाव को हमेशा महसूस करती हूँ इसलिए इस फिल्म की कहानी में नेहमा किस दौर से गुज़र रही है, क्या महसूस कर रही है मुझे समझने में आसानी हुई जबकि नेहमा आत्मविश्वास से भरी स्वछन्द है पर एक झिझक भी साथ हैं जो नेहमा के चरित्र में महसूस कर पाई। शुरुआती दौर में आदिवासी चरित्र के लिए बाहर अभिनेत्री की उपस्थिति के प्रति लोगों की नाराज़गी भी महसूस हुई जो कि कला के किसी माध्यम में पहचान के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए बल्कि चरित्र के प्रति संवेदनशीलता और अभिनय क्षमता केंद्र में होना चाहिए। बहरहाल सारूगरही गाँव के लोगों के साथ काम करके आनंद आया। इस फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में काम करने वाली स्त्रियां उरांव समुदाय की उस गाँव की स्त्रियां हैं। उनके साथ जब संवाद हुआ तो वे अपनी ज़िन्दगी ५ मिनट में सांस रोककर कह डाली। आँखों में जब आंसू छुपाने होते हैं तो उसका गीलापन शब्दों में महसूस हो जाता है। पूरे गाँव के लोग हमारी फिल्म इकाई की सहायता किये। अरण्य पिछले एक वर्ष से बीजू दा (बीजू टोप्पो ) के संपर्क में थे कि वे ट्राइबल समुदाय की जड़ों में बसी छोटी-छोटी बातों को जानना-समझना चाहते थे। जब आदिवासी समुदाय चलता है तो वे विनम्र होकर हर उस छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्हें प्रकृति से मिलती है और यही आदिवासी समुदाय के प्रकृति के साथ सामंजस्य का विरल और अनूठा व्यवहार है।’

तथाकथित विकसित सभ्यता के गुमान में रहने वाले लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है कि आज भी स्त्रियों , बच्चों, दलित,आदिवासी और क्षेत्र विशेष के अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव ,समानता और अन्याय का कभी मौन तो कभी शोरशराबे से भरा अपमान दुनिया के हर हिस्से में जारी है और इसे तथाकथित पढ़े – लिखे लोग स्वीकार कर पाने का साहस नहीं पाते क्योंकि उनके विशेषाधिकार के नज़रिए से या कह लीजिये चश्मे से ये अन्याय दिखाई नहीं देता और खरी बात यह है कि संवेदनशील होने का उनका दायरा सिर्फ अपने तक ही सीमित है। यह हमारे देश में सर्वमान्य है कि जाति और धर्म आधारित हिंसा अब नहीं होती जबकि समाज के हर हिस्से में, हर पल अनगिनत दर्ज़ नहीं की जा सकने वाली प्रताड़नाएं जारी हैं जिसके मूल में श्रेष्ठता बोध का प्रेत नंगा नाचा करता है। तथाकथित सभ्य समाज के सीमित अनुभव दायरे में बतौर उदाहरण एक-दो बराबरी के किस्से हर जगह सुनाए और बताये जाते हैं पर पल – पल होने वाली दुर्भावनाओं, ग़ैर बराबरी से भरे संस्कार ही इस अन्याय की पुष्टि करते हैं। यह सब लिखने के पीछे की मंशा के पीछे हैं इस फिल्म की केंद्रीय भूमिका की नेहमा जिन्हें हम सोनल मधुशंकर के नाम से जानते हैं। सोनल बतौर इंजीनयर हैं और इस पारी के बाद अब वे बतौर कलाकार अपने सपने को सच करने के लिए थियेटर और फिल्म की दुनिया में आई हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोज़ दलित पहचान से आहत होती हैं। अपनी दलित पहचान को हर मंच से कहने के पीछे की मंशा साफ़ है कि समाज अभी भी ग़ैर-बराबरी के रास्ते में फर्राटे से दौड़ना अपनी शान समझता है।
झारखंड में बनीं इस फिल्म में इसके कार्यकारी निर्माता में शामिल हैं सुपरिचित डाक्यूमेंट्री फिल्ममेकर बीजू टोप्पो। उन्होंने जमशेदपुर में स्क्रीनिंग के बाद अपने अनुभव साझा किये –
‘ अरण्य एफ टी आई से पढ़े हैं और पहले उन्हें जानता नहीं था। अरण्य ने मेरा नंबर ढूंढ मुझसे संपर्क किया और मिलने आए, फिल्म बनाने की अनौपचारिक चर्चा की। पहले शॉर्ट फिल्म बनाने का विचार था पर बाद में इस पर काम करते – करते फीचर फिल्म के रूप में यह सामने आई। सबसे पहले जब अरण्य मेरे पास आए तो रील्स में लाल चींटी और कीड़े – मकोड़े को दिखाए और बताये कि वे इन्हें पसंद करते हैं ,मुझे भी समझ नहीं आया कि वे क्या करना चाह रहे हैं। आदिवासी विषय पर अलग तरह से लोग फिल्म बना सकते हैं उन सब बातों पर बात न करके वे चींटी,कीड़े- मकोड़ो पर बात किया करते थे। धीरे-धीरे लोकेशन, चरित्र पर काम किया। सबसे मुश्किल था चरित्रों को ढूंढ निकालना क्योंकि उरांव समुदाय में सिनेमा संस्कृति का हिस्सा नहीं है और सिनेमा ही नहीं बल्कि वे थियेटर भी नहीं करते हैं। जबकि संताल समुदाय जात्रा के संपर्क में रहते हैं और इसलिए जात्रा के प्रभाव से कई लोग संताली फ़िल्में बना भी रहे हैं पर उरांव समुदाय में ऐसा नहीं हैं। इस क्षेत्र में किसी एक को भी ढूंढ निकालना मुश्किल है। कुछ लोगों का नाम दिया पर बातचीत में झिझक रहे थे उन्हें समझा नहीं आ रहा था कि कैसे काम करेंगे तो इसमें काफी दिक्कतें हुई पर अब यह फिल्म मुकम्मल तौर पर आपके सामने आ गई है तो आप देखें ।’

बिना किसी शोरशराबे के प्रकृति के साथ सामंजस्य और सम्मान की भावना से ओतप्रोत ‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म सामाजिक संबंधों पर एक ऐसी दृष्टि विस्तारित करती है जहां मूल में मनुष्य का सम्मान और गरिमा है जिसकी आंच की आभा में हर चरित्र की स्वाभावगत कमियां और खूबियां उजागर होती हैं ,साथ ही समाज के कड़वे यथार्थ से भी परिचय होता है। समाज के हर समुदाय (शहरी और आदिवासी) के यथार्थ को बिना किसी लाग-लपेट के कहने की ऐसी सौंदर्यात्मक व्याख्या विलक्षण है।
बॉलीवुड में करोड़ों – अरबों के बजट वाली फिल्मों के दौर में हिट होने की गारंटी के रेडीमेड फॉर्मूले बिकते हैं और अपनाए जाते हैं जिन्हें देखकर हम उनके खोखलेपन से परिचित होते हैं। एक आम दर्शक भी जानता – समझाता है कि फॉर्मूला फ़िल्में कितनी चलेंगी और उनके फ्लॉप होने की क्या दर है। यह ज़िक्र इसलिए कि ‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म झारखंड के सारूगरही गाँव में फिल्माई गई है जहाँ के निवासी अपनी प्रकृति के साथ फिल्म में शामिल हैं। पूरी फिल्म में कुड़ुख भाषा के गीत हैं जिन्हें स्थानीय गीतकार अपनी आवाज़ देकर अपनी उपस्थिति को दर्ज़ किये हैं। सामान्य तौर पर किसी ऊंचाई तक पहुँचने की यात्रा में माना जाता है कि उस क्षेत्र की मास्टरी ज़रूरी है और यह एक हद तक सच भी है कि तकनीक के लिए अनुभव, अध्ययन और ज्ञान काम आता है पर इसके साथ उस जज़्बे की भी ज़रुरत होती है जो इस विश्वास के साथ आगे बढे कि स्थानीय प्रतिभाओं को किस तरह से बरता जाए कि वे जनमानस की चेतना को झकझोर दें और शोरशराबे,बड़े बजट के बिना भी अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज़ करें जैसे कि ‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म ने किया।
हाल में यह फिल्म ऑस्कर की उस दुनिया में प्रवेश कर गई है जिसके लिए कहा जाता है कि ऑस्कर की रेस या ऑस्कर की दौड़। फिल्म बनाने के बीज का अंकुरण हुआ निर्देशक अरण्य सहाय में और इसको मुकम्मल करने में इसकी पूरी टीम के अथक परिश्रम की झलक फिल्म में मिलती है। निश्चित ही यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए इसके फिल्म निर्माताओं किरण राव और बीजू टोप्पो के साथ पूरी टीम को बधाई।
कला का भूगोल सीमा में बंधा नहीं होता बल्कि वो बनी – बनाई सीमाओं को तोड़ता पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है उसका जीता – जागता उदाहरण है ‘ह्यूमंस इन द लूप’ फिल्म। जिसे देखते हुए महसूस हुआ कि कैसे केंद्र में एक कहानी दुनिया की कहानी बन सकती है वो अपने भूगोल से परे सबकी बात हो जाती है। कला में जब भी केंद्र में मनुष्य, मनुष्यता और समाज के सवाल होंगे तो उसे दुनिया बाहें फैलाए मिलेगी।